पशु-बलि (क़ुरबानी) और इस्लामAuthor Name: मुहम्मद ज़ैनुल-आबिदीन मंसूरी
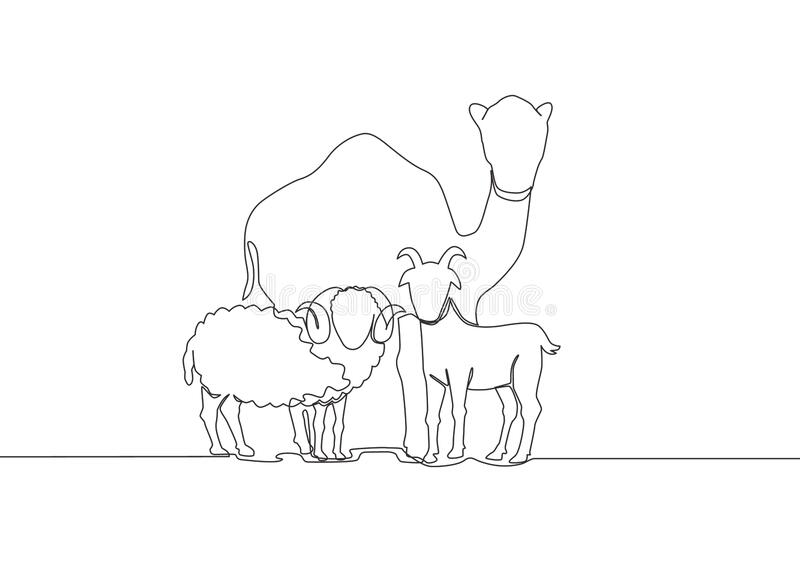
पशु-बलि को विश्व के दो बड़े धर्मों, सनातन धर्म और इस्लाम धर्म में मान्यता प्राप्त है। सनातन धर्म के अनुसार ‘देवताओं को प्रसन्न करने के लिए' और इस्लाम धर्म के अनुसार ‘अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए’ पशु-बलि का विधान है।
इस्लाम में इस्लामी कैलेंडर (हिजरी सन्) के बारहवें मास ‘जिल-हिज्जा’ की दसवीं, ग्यारहवीं व बारहवीं तिथि को ‘ईद-उल-अज़हा’ त्योहार के अवसर पर पशु की बलि दी जाती है जिसे क़ुरबानी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हज को जाने वाले हर व्यक्ति पर भी यह क़ुरबानी अनिवार्य है। विश्व के अन्य भागों मे जानवर की क़ुरबानी करने का सामर्थ्य रखनेवाले हर मुसलमान पर (जो बालिग़ भी हो) क़ुरबानी अनिवार्य है।
यह बलि, निर्दयता व हिंसा का घोतक नहीं है। यह न मात्र पशु-हत्या है, न ही मात्र एक धार्मिक रीति, जिसका कोई महान ध्येय और मनुष्य के जीवन की व्यावहारिकताओं में कोई रचनात्मक भूमिका एवं महत्वपूर्ण योगदान न हो। क़ुरबानी का एक प्रामाणिक व विश्वसनीय इतिहास है जो विश्व के सबसे अधिक प्रामाणिक ईश-ग्रन्थ ‘क़ुरआन’ मे उल्लिखित है तथा जिसकी व्याख्या अंतिम ईश-दूत (पैग़म्बर) हज़रत मुहम्मद (सल.) के अति विश्वसनीय कथनों (हदीस) में वर्णित है।
इतिहास के साथ-साथ इसका असल उद्देश्य भी, इस्लाम के उपरोक्त दोनों मूल-स्त्रोतों में खोल-खोलकर वर्णित कर दिया गया है। इस इतिहास पर एक दृष्टि डाल लेना, क़ुरबानी की इस्लामी अवधारणा को समझने के लिए अनिवार्य है।
हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में स्पष्ट रूप् से पशु-वध की अनुमति तथा आदेश मौजूद हैं। देखें:
मनुस्मृति-3/123, 3/268, 5/23, 5/27-28, 5/35-36
ऋग्वेद-10/27/2, 10/28/3
अथर्ववेद-9/6/4/43/8
शतपथ ब्राह्मण-3/1/2/21
क़ुरबानी का इतिहास
क़ुरबानी का इतिहास 4000 वर्ष पुराना है जिसका आरंभ इस्लाम (तथा यहूदी व ईसाई धर्म) के महान पैग़म्बर हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से संबंधित एक असाधारण घटना से होता है। यह घटना तीनों धर्मों के धर्म-ग्रन्थों में उल्लिखित है।
4000 वर्ष पूर्व जब अज्ञानता के घोर अंधकार में, मानव-जाति निराकार एकेश्वरवाद की सीधी राह से भटक कर साकार अनेकेश्वरवाद की मिथ्या धारणा में फंसी हुई थी। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्रों, तारों, पत्थरों, प्रेतात्माओं, पूर्वजों और शक्तिशाली शासकों की उपासना और मूर्ति-पूजा में लिप्त तथा नाना प्रकार के अंधविश्वासों व आडम्बरों से ग्रस्त थी। अपने से तुच्छ पदार्थों के सामने एवं अपने ही जैसे मनुष्यों के चरणों में शीश नवाते-नवाते मनुष्य की गरिमा, गौरव व स्वाभिमान (जो ईश-प्रदत्त था) अपमानित और छिन्न-भिन्न हो चुका था, तात्कालिक पूरी मानव-जाति में एकेश्वरोपासक एक भी व्यक्ति बाक़ी न रह गया था।
इन विषम परिस्थितियों मे ईराक़ के ‘उर’ नामक नगर के वासी ‘महंत-महापुजारी’ ‘‘आज़र’’ के घर में, उसी के बेटे ‘इब्राहीम' को ईश्वर ने, शिर्क (अनेकेश्वर-पूजा) के घर मे तौहीद( विशुद्ध एकेश्वरवाद) की ज्योति जलाने के लिए चुन लिया और उन्हें अपना पैग़म्बर (ईश-दूत) नियुक्त किया।
हज़रत इब्राहिम ने शिर्क के विरूद्ध ऐसे सशक्त एवं बुद्धिसंगत तर्क दिए जिनकी कोई काट नहीं थी। फिर भी उनका घोर विरोध किया गया। वे इस ज्योति का प्रकाश फ़ैलाने इराक़ से फ़िलिस्तीन, वहाँ से मिस्र और वहाँ से अरब प्रायद्वीप के मध्य-पश्चिम भाग में गए।
अल्लाह ने उनपर एक अत्यन्त कठिन कर्तव्य का भार डाला था। यह कर्तव्य एक ऐसा व्यक्ति ही निभा सकता था जो ईश-आज्ञापालन, ईश-भय, ईशपरायणता एवं ईश्वर के समक्ष संपूर्ण आत्मसमर्पण में उत्कृष्ट, सुदृढ़ और अडिग हो। हर स्वार्थ, सुख, मनोकामना, लाभ, इच्छा और हर तरह के प्रेम की बलि दे सकता हो।
इतना ऊंचा चरित्र और ऐसा सशक्त आत्मबल हज़रत इब्राहीम के व्यक्तित्व में उत्पन्न करने के लिए अल्लाह ने बड़ी-बड़ी कठिनाइयों से गुज़ारकर उन्हे तैयार भी किया, प्रशिक्षण भी दिया और कई कठिन परीक्षाएं भी लीं। हर परीक्षा में हज़रत इब्राहीम स्वंय को उत्तीर्ण सिद्ध करते गए, यहां तक कि ईश्वर ने उनकी अंतिम कठोरतम परीक्षा लेने का इरादा किया। उन्हें आदेश दिया कि (ईश्वर के लिए) अपने पुत्र ‘इस्माईल’ की बलि दें।
इस्माईल (अलैहि.) इब्राहीम (अलैहि.) के इकलौते बेटे थे। वे बड़ी मिन्नत और आरज़ू के बाद इब्राहीम के बुढ़ापे में पैदा हुए थे। अत: सहज ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि इस्माईल, इब्राहीम को कितने अधिक प्रिय और आंखों के तारे रहे होंगे। अत: हज़रत इब्राहीम अपने इकलौते पुत्र इस्माईल से बहुत अधिक प्यार करते थे।
कोई साधारण व्यक्ति होता तो ये बात ईश-आज्ञापालन में अवरोधक बनकर उसके आत्मबल को विचलित कर देने के लिए काफी होती और वह इस कठोर ईश्वरीय परीक्षा में नाकाम हो जाता, लेकिन जिस व्यक्ति से ईश्वर को भावी संसार में इंसानी नस्लों के लिए एकेश्वरवादी धर्म की मजबूत व चिरस्थायी नींव रखवानी थी उस व्यक्ति- हज़रत इब्राहीम ने इस परीक्षा में भी कामयाब होने की ठान ली। बेटे को इस ईश्वरीय आदेश के बारे में बताया तो बेटे (इस्माईल) ने कहा, ‘‘पिताजी, अल्लाह की ओर से जो आदेश हुआ है उसे पूरा कीजिए, ईश्वर ने चाहा तो आप मुझे धैर्यवान और जमे रहनेवाला पाएंगे।‘‘
घर से कुछ दूर ‘मिना’ की एक पहाड़ी पर ले जाकर बाप ने बेटे को लिटा दिया। छुरी गर्दन पर फ़ेरने ही वाले थे कि ईशवाणी हुई कि "ऐ इब्राहीम ! तुम परीक्षा में पूरे उतरे। प्रतिदान के रूप में इस दुंबे (भेड़ समान पशु) की बलि दे दो।" पास ही एक दुंबा खड़ा हुआ मिला। हज़रत इब्राहीम ने उसे क़ुरबान किया। क़ुरआन ने इसे ‘ज़िब्हिन-अज़ीम’ अर्थात् ‘महान बलिदान’ कहा है।
इसी महाबलिदान को याद करने और याद रखने के लिए उसी तिथि को 4000 वर्ष से पशुओं की बलि और क़ुरबानी की रीति चली आ रही है। काल-कालांतर में इसमें कुछ विकृतियां आ गई थीं। लोग इस क़ुरबानी की असल स्पिरिट भी भूल चुके थे।
आज से 1400 वर्ष पूर्व जब पैग़म्बर मुहम्मद (सल.) के माध्यम से विशुद्ध एकेश्वरवादी धर्म का पुनरागमन हुआ और आप (सल.) पर ईशवाणी (क़ुरआन) अवतरित हुई तो क़ुरबानी के इतिहास को भी उसके शुद्ध व स्वच्छ रूप् में लोगों के समक्ष लाया गया। ईश-दूत हज़रत मुहम्मद ने लोगों के सामने इसकी विस्तृत व्याख्या की ओर इस पर स्वंय अमल करके भी दिखाया।
क़ुरआन मे अल्लाह ने फ़रमाया, ‘‘(पशु का) न मांस अल्लाह तक पहुँचता है न रक्त, अपितु उस तक जो चीज़ पहुँचती है वह है तुम्हारा तक़वा (ईशपरायणता)।’’
हज़रत मुहम्मद ने अपनी उंगली सीने पर (हृदय के स्थान पर) रखकर तीन बार फ़रमाया, ‘‘तक़वा यहाँ होता है।’’
'तक़वा' क़ुरआन और हदीस का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका भावार्थ है ‘‘ईश्वर की अवज्ञा (नाफ़रमानी) से बचते हुए जीवन का क्षण-क्षण बिताना’’। अर्थात् कोई भी कार्य करते समय यह ध्यान अवश्य रखना कि कहीं वह ईश्वर की दृष्टि में अनुचित, अवैध, वर्जित और पाप तो नहीं है (अनुचित, अवैध और पाप होने की पूरी व्याख्या क़ुरआन और हदीस में उल्लिखित है)। अगर किसी काम में अल्लाह की नाफ़रमानी व अवज्ञा है तो उसपर अमल करना छोड़ देने को भी इस्लामी परिभाषा में ‘तक़वा’ कहते हैं।
निष्कर्ष
उपरोक्त विवरण का निष्कर्ष यह है:
सृष्टि के सृजनकर्ता, अल्लाह ने पृथ्वी की सारी जीवधारी वस्तुएं मनुष्य के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उपयोग के लिए बनाई हैं। उपभोग मे ‘मांसाहार’ भी आता है एवं इसे इस्लामी व ग़ैर-इस्लामी समाजों में समान रूप से मान्यता प्राप्त है। कुछ व्यक्तिगत या सीमित सामुदायिक अपवाद भी हैं, जो नगण्य हैं।
इस्लामी समाज में प्रचलित पशु-बलि (क़ुरबानी) का एक उत्कृष्ट व पवित्र इतिहास है। 1400 वर्ष से प्रतिवर्ष उसी इतिहास की याद ताजा की जाती है और मुस्लिम-समाज इस क़ुरबानी के माध्यम से अपने और अल्लाह के बीच ‘दास’ व ‘स्वामी’ के संबंध को घनिष्ट व दृढ़ करता है।
क़ुरबानी के माध्यम से एक मुस्लिम व्यक्ति प्रयास करता है कि अपने अन्दर ईश-भय (तक़वा) के गुण को उन्नति व वृद्धि दे। बुरे और पाप के कामों से बचे।
क़ुरबानी के माध्यम से एक मुस्लिम व्यक्ति अपने अन्दर यह आत्मबल पैदा करने की आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करता है कि सत्यनिष्ठ जीवन बिताने के लिए तथा ईश आज्ञापालन मे वह बड़े से बड़े स्वार्थ, लाभ, हित और भावनाओं की क़ुरबानी दे सके और सत्य-मार्ग से विचलित कदापि न हो।
जीव-हत्या अपने में न तो सही है न ग़लत, न उचित है न अनुचित, न निन्दनीय है न सराहनीय। यह बात यूँ भी कही जा सकती है कि जीव-हत्या अपने आप मे सही भी है, और ग़लत भी। सही या ग़लत होना इस बात पर निर्भर है कि जीव-हत्या का ‘उद्देश्य’ क्या है और जीव-हत्या के संबंध में इस्लामी दृष्टिकोण भी यही है।
मिसाल के तौर पर एक जीवित मेंढक की अनर्थ हत्या करके उसे फेंक दिया जाए तो यह इस्लाम की दृष्टि में निर्दयता, हिंसा एवं पाप है लेकिन चिकित्सा-विज्ञान के विद्यार्थियों को शल्य-प्रशिक्षण (Surgical Training) देने के लिए उनके द्वारा मेडिकल-कालेजों में जो मेंढकों को चीरा-फ़ाड़ा जाता है वह निरर्थक व व्यर्थ कार्य न होकर मनुष्य व मानव-जाति की सेवा के लिए होता हैं इसीलिए यह न निर्दयता है, न हिंसा, न पाप; बल्कि लाभदायक, वांछनीय व सराहनीय है।
हमारा विश्वास है कि हत्या व हिंसा के उचित या अनुचित होने का यही मापदण्ड, सम्पूर्ण मानव समाज में, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक मान्य व प्रचलित रहा है। यही मानव-प्रकृति के भी अनुकूल है और मानव-जीवन की स्वाभाविक आवश्यकताओं के तकाजों (Requisites) के अनुकूल भी। क्योंकि इस्लाम एक स्वाभाविक व प्राकृतिक धर्म है, इसीलिए वह उपरोक्त बौद्धिक, संतुलित और स्वाभाविक वैश्विक सिद्धान्त का पक्षधर है।